सती-1 मुंशी प्रेमचंद की कहानी | Sati Premchand Best Hindi Story
सती-1 Munshi Premchand मुंशी प्रेमचंद | प्रेमचंद की कहानियाँ | मुंशी प्रेमचंद की सर्वश्रेष्ठ कहानियां
Sati Munshi Premchand kahani Hindi:दो शताब्दियों से अधिक बीत गये हैं; पर चिंतादेवी का नाम चला आता है। बुंदेलखंड के एक बीहड़-स्थान में आज भी मंगलवार को सहस्रों स्त्री-पुरुष चिंतादेवी की पूजा करने आते हैं। उस दिन यह निर्जन स्थान सुहाने गीतों से गूंज उठता है, टीले और टोकरे रमणियों के रंग-बिरंगे वस्त्रों से सुशोभित हो जाते हैं। देवी का मंदिर एक बहुत ऊंचे टीले पर बना हुआ है। उसके कलश पर लहराती हुई लाल पताका बहुत दूर से दिखायी देती है। मन्दिर इतना छोटा है कि उसमें मुश्किल से एक साथ दो आदमी समा सकते हैं। भीतर कोई प्रतिमा नहीं है, केवल एक छोटी-सी वेदी बनी हुई है। नीचे से मन्दिर तक पत्थर का जीना है। भीड़-भाड़ में धक्का खाकर कोई नीचे न गिर पड़े, इसलिए जीने की दीवार दोनों तरफ बनी हुई है। यहीं चिंतादेवी सती हुई थीं; पर लोकरीति के अनुसार वह अपने मृत पति के साथ चिता पर बैठी थीं। उनका पति हाथ जोड़े सामने खड़ा था; पर वह उसकी ओर आंखें उठाकर भी न देखती थी। वह पति के शरीर के साथ नहीं, उसकी आत्मा के साथ सती हुई। उस चिता पर पति का शरीर न था, उसकी मर्यादा भस्सीभूत हो रही थी।
यमुना तट पर एक छोटा-सा नगर है। चिंता उसी नगर के एक वीर बुन्देल की कन्या थी। उसकी माता उसकी बाल्यावस्था में ही परलोक सिधार चुकी थी। उसके पालन-पोषण का भार पिता पर पड़ा। संग्राम का समय था, योद्धाओं को कमर खोलने की भी फुरसत न मिलती थी, वे घोड़े की पीठ पर भोजन करते और जीन ही पर झपकियां ले लेते थे । चिंता का बाल्यकाल पिता के साथ समरभूमि में कटा । बाप उसे किसी खोह में या वृक्ष की आड़ में छिपा कर मैदान में चला जाता। चिंता निश्शंक भाव से बैठी हुई मिट्टी के किले बनाती और बिगाड़ती। उसके घरौंदे थे, उसकी गुड़ियां ओढ़नी न ओढ़ती थीं। वह सिपाहियों के गुड्डे बनाती और उन्हें रण-क्षेत्र में खड़ा करती थी।
कभी-कभी उसका पिता संध्या समय भी न लौटता; पर चिंता को भय छू तक न गया था। निर्जन स्थान में भूखी-प्यासी रात-रात भर बैठी रह जाती। उसने नेवले और सियार की कहानियां कभी न सुनी थीं। वीरों के आत्मोत्सर्ग की कहानियां, और वह भी योद्धाओं के मुंह से सुन-सुन कर वह आदर्शवादिनी बन गयी थी।एक एक बार तीन दिन तक चिंता को अपने पिता की खबर न मिली। वह एक पहाड़ी की खोह में बैठी मन ही मन एक ऐसा किला बना रही थी, जिसे शत्रु किसी भांति जान न सके। दिन भर वह उसी किले का नक्शा सोचती और रात को उसी किले का स्वप्न देखती।
तीसरे दिन संध्या-समय उसके पिता के कई साथियों ने आकर उसके सामने रोना शुरू किया। चिंता ने विस्मित होकर पूछा-दादा जी कहां हैं? तुम लोग क्यों रोते हो?
किसी ने इसका उत्तर न दिया। वे जोर से धाड़े मार-मारकर रोने लगे। चिंता समझ गयी कि उसके पिता ने वीरगति पायी। इस तेरह वर्ष की बालिका की आंखों से आंसू की एक बूंद भी न गिरी, मुख जरा भी मलिन न हुआ, एक आह भी न निकली। हंस कर बोली- अगर उन्होंने वीरगति पायी, तो तुम लोग रोते क्यों हो ? योद्धाओं के लिए इससे बढ़ कर और कौन सी मृत्यु हो सकती है ? इससे बढ़कर उनकी वीरता का और क्या पुरस्कार मिल सकता है ? यह रोने का नहीं, आनन्द मनाने का अवसर है।
एक सिपाही ने चिंतित स्वर में कहा-हमें तुम्हारी चिंता है। तुम अब कहां रहोगी?
चिंता ने गम्भीरता से कहा-इसकी तुम कुछ चिंता न करो, दादा! मैं अपने बाप की बेटी हूं। जो कुछ उन्होंने किया, वही मैं करूंगी। अपनी मातृभूमि को शत्रुओं के पंजे से छुड़ाने में उन्होंने प्राण दे दिये। मेरे सामने भी वही आदर्श है। जा कर अपने आदमियों को संभालिए। मेरे लिए एक घोड़ा और हथियारों का प्रबन्ध कर दीजिए। ईश्वर ने चाहा तो आप लोग मुझे किसी से पीछे न पायेंगे, लेकिन यदि मुझे पीछे हटते देखना, तो तलवार के एक हाथ से इस जीवन का अंत कर देना। यही मेरी आपसे विनय है। जाइए अब विलम्ब न कीजिए।
Read More:
- गुप्तधन: कहानी मुंशी प्रेमचंद
- शतरंज के खिलाड़ी: मुंशी प्रेमचंद कहानी
- वैर का अंत: मुंशी प्रेमचंद कहानी
- सत्याग्रह: मुंशी प्रेमचंद कहानी
- नैराश्य लीला: मुंशी प्रेमचंद कहानी
- रामलीला:प्रेमचंद की कहानी
सिपाहियों को चिंता के ये वीर-वचन सुनकर कुछ भी आश्चर्य नहीं हुआ। हां, उन्हें यह संदेह अवश्य हुआ कि क्या कोमल बालिका अपने संकल्प पर दृढ़ रह सकेगी ?
पांच वर्ष बीत गये। समस्त प्रांत में चिंता देवी की धाक बैठ गई। शत्रुओं के कदम उखड़ गये। वह विजय की सजीव मूर्ति थी, उसे तीरों और गोलियों के सामने निश्शंक खड़े देखकर सिपाहियों को उत्तेजना मिलती रहती थी। उसके सामने वे कैसे कदम पीछे हटाते ? कोमलांगी युवती आगे बढ़े तो कौन पुरुष पीछे हटेगा ! सुंदरियों के सम्मुख योद्धाओं की वीरता अजेय हो जाती है। रमणी के वचन-बाण योद्धाओं के लिये आत्म-समर्पण के गुप्त संदेश हैं। उसकी एक चितवन कायरों में भी पुरुषत्व प्रवाहित कर देती है। चिंता की छवि कीर्ति ने मनचले सूरमाओं को चारों ओर से खींच-खींच कर उसकी सेना को सजा दिया - जान पर खेलने वाले भौरे चारों ओर से आ-आ कर इस फूल पर मंडराने लगे।
इन्हीं योद्धाओं में रत्नसिंह नाम का एक युवक राजपूत भी था।
यों तो चिंता के सैनिकों में सभी तलवार के धनी थे; बात पर जान देने वाले, उसके इशारे पर आग में कूदने वाले, उसकी आज्ञा पा कर एक बार आकाश के तारे तोड़ लाने को भी चल पड़ते; किन्तु रत्नसिंह सबसे बढ़ा हुआ था। चिंता भी हृदय में उससे प्रेम करती थी। रत्नसिंह अन्य वीरों की भांति अक्खड़, मुंहफट या घमंडी न था। और लोग अपनी-अपनी कीर्ति को खूब बढ़ा-बढ़ा कर बयान करते, आत्म-प्रशंसा करते हुए उनकी जबान न रुकती थी। वे जो कुछ करते, चिंता को दिखाने के लिए। उनका ध्येय अपना कर्त्तव्य न था, चिंता थी। रत्नसिंह जो कुछ करता, शांत भाव से। अपनी प्रशंसा करना तो दूर रहा, वह चाहे कोई शेर को क्यों न मार आये, उसकी चर्चा तक न करता। उसकी विनयशीलता और नम्रता, संकोच की सीमा से भिड़ गयी थी। औरों के प्रेम में विलास था; पर रत्नसिंह के प्रेम में त्याग और तप और लोग मीठी नींद सोते थे; पर रत्नसिंह तारे गिन-गिन कर रात काटता था और सब अपने दिल में समझते थे कि चिंता मेरी होगी-केवल रत्नसिंह निराश था, और इसलिए उसे किसी से न द्वेष था, न राग औरों को चिंता के सामने चहकते देखकर उसे उनकी वाक्पटुता पर आश्चर्य होता, प्रतिक्षण उसका निराशांधकार और भी घना हो जाता था। कभी- कभी वह अपने बोदेपन पर झुंझला उठता- क्यों ईश्वर ने उसे उन गुणों से वंचित रखा, जो रमणियों के चित्त को मोहित करते हैं? उसे कौन पूछेगा ? उसकी मनोव्यथा को कौन जानता है ? पर वह मन में झुंझला कर रह जाता था। दिखावे की उसकी सामर्थ्य ही न थी।
आधी से अधिक रात बीत चुकी थी। चिंता अपने खेमे में विश्राम कर रही थी। सैनिकगण भी कड़ी मंजिल मारने के बाद कुछ खा-पी कर गाफिल पड़े हुए थे। आगे एक घना जंगल था। जंगल के उस पार शत्रुओं का एक दल डेरा डाले पड़ा था। चिंता उसके आने की खबर पाकर भागमभाग चली आ रही थी। उसने प्रातः काल शत्रुओं पर धावा करने का निश्चय कर लिया था। उसे विश्वास था कि शत्रुओं को मेरे आने की खबर न होगी; किन्तु यह उसका भ्रम था। उसी की सेना का एक आदमी शत्रुओं से मिला हुआ था। यहां की खबरें वहां नित्य पहुंचती रहती थीं। उन्होंने चिंता से निश्चिंत होने के लिए एक षड्यंत्र रच रखा था - उसकी गुप्त हत्या करने के लिए तीन साहसी सिपाहियों को नियुक्त कर दिया था। वे तीनों हिंस्र पशुओं की भांति दबे पांव जंगल को पार करके आये और वृक्षों की आड़ में खड़े होकर सोचने लगे कि चिंता का खेमा कौन-सा है ? सारी सेना बेखबर सो रही थी, इससे उन्हें अपने कार्य की सिद्धि में लेशमात्र संदेह न था। वे वृक्षों की आड़ से निकले, और जमीन पर मगर की तरह रेंगते हुए चिंता के खेमे की ओर चले।
सारी सेना बे-खबर सोती थी, पहरे के सिपाही थक कर चूर हो जाने के कारण निद्रा में मग्न हो गये हैं। केवल एक प्राणी खेमे के पीछे मारे ठंड के सिकुड़ा हुआ बैठा था। यही रत्नसिंह था। आज उसने यह कोई नयी बात न की थी। पड़ावों में उसकी रातें इसी भांति चिंता के खेमे के पीछे बैठे-बैठे कटती थीं। घातकों की आहट पाकर उसने तलवार निकाल ली, और चौंक कर उठ खड़ा हुआ। देखा-तीन आदमी झुके हुए चले आ रहे हैं। अब क्या करे? अगर शोर मचाता है, तो सेना में खलबली पड़ जाय, और अंधेरे में लोग एक दूसरे पर वार करके आपस ही में कट मरें। इधर अकेले तीन जवानों से भिड़ने में प्राणों का भय । अधिक सोचने का मौका न था। उसमें योद्धाओं की अविलम्ब निश्चय कर लेने की शक्ति थी; तुरन्त तलवार खींच ली, और उन तीनों पर टूट पड़ा। कई मिनट तक तलवारें छपाछप चलती रहीं। फिर सन्नाटा छा गया। उधर वे तीनों आहत हो कर गिर पड़े, इधर यह भी जख्मों चूर हो कर अचेत हो गया।
प्रातःकाल चिंता उठी, तो चारों जवानों को भूमि पर पड़े पाया। उसका कलेजा धक् से हो गया। समीप जा कर देखा - तीनों आक्रमणकारियों के प्राण निकल चुके थे; पर रत्नसिंह की सांस चल रही थी। सारी घटना समझ में आ गयी। नारीत्व ने वीरत्व पर विजय पायी।
जिन आंखों से पिता की मृत्यु पर आंसू की एक बूंद भी न गिरी थी, उन्हीं आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गयी। उसने रत्नसिंह का सिर अपनी जांघ पर रख लिया, और हृदयांगण में रचे हुए स्वयंवर में उसके गले में जयमाल डाल दी।
महीने भर न रत्नसिंह की आंखें खुलीं और न चिंता की आंखें बन्द हुई। चिंता उसके पास से एक क्षण के लिए भी कहीं न जाती। न अपने इलाके की परवा थी, न शत्रुओं के बढ़ते चले आने की फिक्र। रत्नसिंह की आंखें खुलीं। देखा― चारपाई पर पड़ा हुआ है, और चिंता सामने पंखा लिए खड़ी है। क्षीण स्वर में बोला- चिंता, पंखा मुझे दे दो, तुम्हें कष्ट हो रहा है।
चिंता का हृदय इस समय स्वर्ग के अखंड, अपार सुख का अनुभव कर रहा था। एक महीना पहले जिस जीर्ण शरीर के सिरहाने बैठी हुई वह नैराश्य से रोया करती थी, उसे आज बोलते देख कर आह्लाद का पारावार न था। उसने स्नेह-मधुर स्वर में कहा- प्राणनाथ, यदि यह कष्ट है, तो सुख क्या है, मैं नहीं जानती। 'प्राणनाथ' - सम्बोधन में विलक्षण मंत्र की- सी शक्ति थी । रत्नसिंह की आंखें चमक उठीं। जीर्ण मुद्रा प्रदीप्त हो गयी, नसों में एक नये जीवन का संचार हो उठा, और वह जीवन कितना स्फूर्तिमय था। उसमें कितना उत्साह, कितना माधुर्य, कितना उल्लास और कितनी करुणा थी । रत्नसिंह के अंग-अंग फड़कने लगे। उसे अपनी भुजाओं में अलौकिक पराक्रम का अनुभव होने लगा। ऐसा जान पड़ा, मानो वह सारे संसार को सर कर सकता है, उड़ कर आकाश पर पहुंच सकता है, पर्वतों को चीर सकता है। एक क्षण के लिए उसे ऐसी तृप्ति हुई, मानो उसकी सारी अभिलाषाएं पूरी हो गयी हैं, और वह अब किसी से कुछ नहीं चाहता; शायद शिव को सामने खड़े देखकर भी वह मुंह फेर लेगा, कोई वरदान न मांगेगा। उसे अब किसी ऋद्धि की, किसी पदार्थ की इच्छा न थी। उसे गर्व हो रहा था, मानो उससे अधिक सुखी, उससे अधिक भाग्यशाली पुरुष संसार में और कोई न होगा।
Read More:
- शंखनाद कहानी प्रेमचंद
- ब्रह्म का स्वांग: कहानी प्रेमचंद
- शान्ति-1: कहानी मुंशी प्रेमचंद
- परीक्षा-2 कहानी मुंशी प्रेमचंद
चिंता अभी अपना वाक्य पूरा भी न कर पायी थी कि उसी प्रसंग में बोली- हां, आपको मेरे कारण अलबत्ता दुस्सह यातना भोगना पड़ी।
रत्नसिंह ने उठने की चेष्टा करके कहा- बिना तप के सिद्धि नहीं मिलती।
चिंता ने रत्नसिंह को कोमल हाथों से लिटाते हुए कहा-इस सिद्धि के लिए तुमने तपस्या नहीं की थी। झूठ क्यों बोलते हो? तुम केवल एक अबला की रक्षा कर रहे थे। यदि मेरी जगह कोई दूसरी स्त्री होती, तो भी तुम इतने ही प्राणप्रण से उसकी रक्षा करते। मुझे इसका विश्वास है। मैं तुमसे सत्य कहती हूं, मैंने ब्रह्मचारिणी रहने का प्रण कर लिया था; लेकिन तुम्हारे आत्मोत्सर्ग ने मेरे प्रण को तोड डाला। मेरा पालन योद्धाओं की गोद में हुआ है; मेरा हृदय उसी पुरुषसिंह के चरणों में अर्पण हो सकता है, जो प्राणों की बाजी खेल सकता हो । रसिकों के हास-विलास, गुंडों के रूप-रंग और फेकैतों से दांव-घात का मेरी दृष्टि में रत्ती भर भी मूल्य नहीं। उनकी नट-विद्या को मैं केवल तमाशे की तरह देखती हूं। तुम्हारे ही हृदय में मैंने सच्चा उत्सर्ग पाया, और तुम्हारी दासी हो गयी-आज से नहीं, बहुत दिनों से।
प्रणय की पहली रात थी— चारों ओर सन्नाटा था। केवल दोनों प्रेमियों के हृदयों में अभिलाषाएं लहरा रही थीं। चारों ओर अनुरागमयी चांदनी छिटकी हुई थी, और उसकी हास्यमयी छटा में वर-वधू प्रेमालाप कर रहे थे।
सहसा खबर आयी कि शत्रुओं की एक सेना किले की ओर बढ़ी चली आती है। चिंता चौंक पड़ी; रत्नसिंह खड़ा हो गया, और खूंटी से लटकती हुई तलवार उतार ली।
चिंता ने उसकी ओर कातर स्नेह की दृष्टि से देखकर कहा- कुछ आदमियों को उधर भेज दो, तुम्हारे जाने की क्या जरूरत है ?
रत्नसिंह ने बंदूक कंधे पर रखते हुए कहा-मुझे भय है कि अबकी वे लोग बड़ी संख्या में आ रहे हैं।
चिंता - तो मैं भी चलूंगी।
नहीं, मुझे आशा है, वे लोग ठहर न सकेंगे। मैं एक ही धावे में अनेक कदम उखाड़ दूंगा। यह ईश्वर की इच्छा है कि हमारी प्रणय-रात्रि विजय-रात्रि हो !
'न जाने क्यों मन कातर हो रहा है। जाने देने को जी नहीं चाहता!'
रत्नसिंह ने इस सरल, अनुरक्त आग्रह से विह्वल होकर चिंता को गले लगा लिया और बोले-मैं सवेरे तक लौट आऊंगा, प्रिये!
चिंता पति के गले में हाथ डालकर आंखों में आंसू भरे हुए बोली- मुझे भय है, तुम बहुत दिनों में लौटोगे। मेरा मन तुम्हारे साथ रहेगा। जाओ, पर रोज खबर भेजते रहना। तुम्हारे पैरों पड़ती हूं, अवसर का विचार करके धावा करना। तुम्हारी आदत है कि शत्रु देखते ही आकुल हो जाते हो, और जान पर खेल कर टूट पड़ते हो। तुमसे मेरा यही अनुरोध है कि अवसर देखकर काम करना । जाओ जिस तरह पीठ दिखाते हो, उसी तरह मुंह दिखाओ।
चिंता का हृदय कातर हो रहा था। वहां पहले केवल विजय-लालसा का आधिपत्य था, अब भोग-लालसा की प्रधानता थी। वही वीर बाला, जो सिंहनी की तरह गरज कर शत्रुओं के कलेजे को कंपा देती थी, आज इतनी दुर्बल हो रही थी कि जब रत्नसिंह घोड़े पर सवार हुआ, तो आप उसकी कुशल-कामना से मन ही मन देवी की मनौतियां कर रही थी। जब तक वह वृक्षों की ओट में छिप न गया, वह खड़ी उसे देखती रही, फिर वह किले के सबसे ऊंचे बुर्ज पर चढ़ गयी, और घंटों उसी तरफ ताकती रही। वहां शून्य था, पहाड़ियों ने कभी का रत्नसिंह को अपनी ओट में छिपा लिया था; पर चिंता को ऐसे जान पड़ा था कि वह सामने चले आ रहे हैं। अब ऊषा की लोहित छवि वृक्षों की आड़ से झांकने लगी, तो उसकी मोह विस्मृति टूट गयी। मालूम हुआ, चारों तरफ शून्य है। वह रोती हुई बुर्ज से उतरी, और शय्या पर मुंह ढांप कर रोने लगी।
रत्नसिंह के साथ मुश्किल से सौ आदमी थे; किन्तु सभी मंजे हुए, अवसर और संख्या को तुच्छ समझने वाले, अपनी जान के दुश्मन ! वीरोल्लास से भरे हुए, एक वीर रस पूर्ण पद गाते हुए घोड़ों को बढ़ाये चले जाते थे-
'बांकी तेरी पाग सिपाही, इसकी रखना लाज।
तेग-तवर कुछ काम न आये, बख्तर-ढाल व्यर्थ हो जावे।
रखियो मन में लाग, सिपाही बांकी तेरी पाग।
इसकी रखना लाज॥'
पहाड़ियां इन वीर स्वरों से गूंज रही थीं। घोड़ों की टाप ताल दे रही थी। यहां तक कि रात बीत गयी, सूर्य ने अपनी लाल आंखें खोल दी और उन वीरों पर अपनी स्वर्ण-छटा की वर्षा करने लगा।
वहीं रक्तमय प्रकाश में शत्रुओं की सेना एक पहाड़ी पर पड़ाव डाले हुए नजर आयी। रत्नसिंह सिर झुकाये, वियोग-व्यथित हृदय को दबाये, मन्द गति से पीछे-पीछे चला जाता था। कदम आगे बढ़ता था, पर मन पीछे हटता। आज जीवन में पहली बार दुश्चिंताओं ने उसे आशंकित कर रखा था। कौन जानता है, लड़ाई का अंत क्या होगा ? जिस स्वर्ग-सुख को छोड़ कर वह आया था, उसकी स्मृतियां रह रह कर उसके हृदय को मसोस रही थीं; चिंता की सजल आंखें याद आती थीं और जी चाहता था, घोड़े की रास पीछे मोड़ दे। प्रतिक्षण रणोत्साह क्षीण होता जाता था, सहसा एक सरदार ने समीप आ कर कहा- भैया, यह देखो, ऊंची पहाड़ी पर शत्रु डेरे डाले पड़े हैं। तुम्हारी अब क्या राय है? हमारी तो यह इच्छा है कि तुरन्त उन पर धावा कर दें। गाफिल पड़े हुए हैं, भाग खड़े होंगे। देर करने से वे भी संभल जायेंगे और तब मामला नाजुक हो जायगा । एक हजार से कम न होंगे।
रत्नसिंह ने चिंतित नेत्रों से शत्रु दल की ओर देख कर कहा-हां, मालूम तो होता है।
सिपाही - तो धावा कर दिया जाय न ?
रत्नसिंह - जैसी तुम्हारी इच्छा। संख्या अधिक है, यह सोच लो।
सिपाही - इसकी परवाह नहीं। हम इससे बड़ी सेनाओं को परास्त कर चुके हैं।
रत्नसिंह - यह सच है; पर आग में कूदना ठीक नहीं।
सिपाही - भैया, तुम कहते क्या हो ? सिपाही का तो जीवन ही आग में कूदने के लिए है। तुम्हारे हुक्म की देर है, फिर हमारा जीवन देखना।
रत्नसिंह-अभी हम लोग बहुत थके हुए हैं। जरा विश्राम कर लेना अच्छा है।
सिपाही – नहीं भैया; उन सबों को हमारी आहट मिल गयी, तो गजब हो जाएगा।
रत्नसिंह - तो फिर धावा ही कर दो।
एक क्षण में योद्धाओं ने घोड़ों की बागें उठा दीं, और अस्त्र संभाले हुए शत्रु सेना पर लपके; किन्तु पहाड़ी पर पहुंचते ही इन लोगों ने उसके विषय में जो अनुमान किया था, वह मिथ्या था। वह सजग ही न थे स्वयं किले पर धावा करने की तैयारियां भी कर रहे थे। इन लोगों ने जब उन्हें सामने आते देखा, तो समझ गये कि भूल हुई; लेकिन अब सामना करने के सिवा चारा ही क्या था। फिर भी वे निराश न थे। रत्नसिंह जैसे कुशल योद्धा के साथ इन्हें कोई शंका नहीं थी। वह इससे भी कठिन अवसरों पर अपने रण-कौशल से विजय- लाभ कर चुका था। क्या आज वह अपना जौहर न दिखाएगा ? सारी आंखें रत्नसिंह को खोज रही थीं; पर उसका वहां कहीं पता न था। कहां चला गया? यह कोई न जानता था।
पर वह कहीं नहीं जा सकता। अपने साथियों को इस कठिन अवस्था में छोड़कर वह कहीं नहीं जा सकता—सम्भव नहीं। अवश्य ही वह यहीं है और हारी हुई बाजी को जिताने की कोई युक्ति सोच रहा है।
एक क्षण में शत्रु इनके सामने आ पहुंचे। इतनी बहुसंख्यक सेना के सामने ये मुट्ठी भर आदमी क्या कर सकते थे। चारों ओर से रत्नसिंह की पुकार होने लगी- भैया, तुम कहां हो? हमें क्या हुक्म देते हो? देखते हो, वे लोग सामने आ पहुंचे; पर तुम अभी मौन खड़े हो। सामने आकर हमें मार्ग दिखाओ, हमारा उत्साह बढ़ाओ !
पर अब भी रत्नसिंह न दिखायी दिया। यहां तक कि शत्रु-दल सिर पर आ पहुंचा, और दोनों दलों में तलवारें चलने लगीं। बुन्देलों ने प्राण हथेली पर ले कर लड़ना शुरू किया; पर एक को एक बहुत होता है; एक और दस का मुकाबिला ही क्या? यह लड़ाई न थी, प्राणों का जुआ था! बुन्देलों में निराशा का अलौकिक बल था। खूब लड़े पर क्या मजाल कि कदम पीछे हटे। उनमें अब जरा भी संगठन न था। जिससे जितना आगे बढ़ते बना बढ़ा। अंत क्या होगा, इसकी किसी को चिंता न थी। कोई तो शत्रुओं की सर्फे चीरता हुआ सेनापति के समीप पहुंच गया, कोई उनके हाथी पर चढ़ने की चेष्टा करते मारा गया। उनका अमानुषिक साहस देखकर शत्रुओं के मुंह से भी वाह-वाह निकलती थी; लेकिन ऐसे योद्धाओं ने नाम पाया है, विजय नहीं पायी। एक घंटे में रंगमंच का परदा गिर गया, तमाशा खतम हो गया। एक आधी थी; जो आयी और वृक्षों को उखाड़ती हुई चली गयी। संगठित रह कर ये मुट्ठी भर आदमी दुश्मनों के दांत खट्टे कर देते; पर जिस पर संगठन का भार था, उसका कहीं पता न था। विजयी मराठों ने एक-एक लाश ध्यान से देखी । रत्नसिंह उनकी आंखों में खटकता था। उसी पर उनके दांत लगे थे। रत्नसिंह के जीते- जी उन्हें नींद न आती थी। लोगों ने पहाड़ी की एक-एक चट्टान का मन्थन कर डाला; पर रत्न न हाथ आया। विजय हुई; पर अधूरी।
चिंता के हृदय में आज न जाने क्यों भांति-भांति की शंकाएं उठ रही थीं वह कभी इतनी दुर्बल न थी। बुन्देलों की हार ही क्यों होगी, इसका कोई कारण तो वह न बता सकती थी; पर यह भावना उसके विकल हृदय से किसी तरह न निकलती थी। उस अभागिन के भाग्य में प्रेम का सुख भोगना लिखा होता, तो क्या बचपन ही में मां मर जाती, पिता के साथ वन- वन घूमना पड़ता, खोहों और कंदराओं में रहना पड़ता। और वह आश्रय भी तो बहुत दिन न रहा। पिता भी मुंह मोड़ कर चल दिये। तब से उसे एक दिन भी तो आराम से बैठना नसीब न हुआ। विधा क्या अब अपना क्रूर कौतुक छोड़ देगा? आह ! उसके दुर्बल हृदय में इस समय एक विचित्र भावना उत्पन्न हुई-ईश्वर उसके प्रियतम को आज सकुशल लाये, तो वह उसे लेकर किसी दूर के गांव में जा बसेगी। पतिदेव की सेवा और आराधना में जीवन सफल करेगी। इस संग्राम से सदा के लिए मुंह मोड़ लेगी। आज पहली बार नारीत्व का भाव उसके मन में जाग्रत हुआ।
संध्या हो गयी थी, सूर्य भगवान् किसी हारे हुए सिपाही की भांति मस्तक झुकाते कोई आड़ खोज रहे थे। सहसा एक सिपाही नंगे सिर, पांव, निरस्त्र उसके सामने आ कर खड़ा हो गया। चिंता पर वज्रपात हो गया। एक क्षण तक मर्माहत सी बैठी रही। फिर उठ कर घबराई हुई सैनिक के पास आयी, और आतुर स्वर में पूछा-कौन-कौन बचा?
सैनिक ने कहा- कोई नहीं।
'कोई नहीं ? कोई नहीं ?
चिंता सिर पकड़ कर भूमि पर बैठ गयी। सैनिक ने फिर कहा-मरहठे समीप आ पहुंचे।
'समीप आ पहुंचे ?'
"बहुत समीप!"
"तो तुरंत चिता तैयार करो। समय नहीं है।'
अभी हम लोग तो सिर कटाने को हाजिर हो हैं।'
"तुम्हारी जैसी इच्छा। मेरे कर्त्तव्य का तो यही अंत है।'
'किला बंद करके हम महीनों लड़ सकते हैं।'
'तो जाकर लड़ो। मेरी लड़ाई अब किसी से नहीं।'
एक ओर अंधकार प्रकाश को पैरों तले कुचलता चला आता था; दूसरी ओर विजयी मरहठे लहराते हुए खेतों को और किले में चिता बन रही थी। ज्यों ही दीपक जले, चिता में भी आग लगी। सती चिंता सोलहो श्रृंगार किये, अनुपम छवि दिखाती हुई, प्रसन्न मुख अग्नि-मार्ग से पतिलोक की यात्रा करने जा रही थी।
चिता के चारों ओर स्त्री और पुरुष जमा थे। शत्रुओं ने किले को घेर लिया है इसकी किसी को फिक्र न थी। शोक और संतोष से सबके चेहरे उदास और सिर झुके हुए थे। अभी कल इसी आंगन में विवाह का मंडप सजाया गया था। जहां इस समय चिता सुलग रही है, वहीं कल हवन कुण्ड था। कल भी इसी भांति अग्नि की लपटें उठ रही थीं, इसी भांति लोग जमा थे; पर आज और कल के दृश्यों में कितना अंतर है! हां स्थूल नेत्रों के लिए अंतर हो सकता है; पर वास्तव में यह उसी यज्ञ की पूर्णाहुति हैं, उसी प्रतिज्ञा का पालन है।
सहसा घोड़े की टापों की आवाजें सुनायी देने लगीं। मालूम होता था, कोई सिपाही घोड़े को सरपट भगाता चला आ रहा है। एक क्षण में टापों की आवाज बंद हो गयी, और एक सैनिक आंगन में दौड़ा हुआ आ पहुंचा। लोगों ने चकित होकर देखा, यह रत्नसिंह था ।
रत्नसिंह चिता के पास जाकर हांफता हुआ बोला- प्रिय, मैं तो अभी जीवित हूं, यह तुमने क्या कर डाला ?
चिता में आग लग चुकी थी। चिंता की साड़ी में से अग्नि की ज्वाला निकल रही थी। रत्नसिंह उन्मत्त की भांति चिता में घुस गया, और चिंता का हाथ पकड़ कर उठाने लगा। लोगों ने चारों ओर से लपक लपक कर चिता की लकड़ियां हटानी शुरू कीं; पर चिंता ने पति की ओर आंख उठा कर भी न देखा, केवल हाथों से हट जाने का संकेत किया।
रत्नसिंह सिर पीट कर बोला- हाय प्रिये, तुम्हें क्या हो गया है। मेरी ओर देखती क्यों नहीं? मैं तो जीवित हूं।
चिता से आवाज आयी - तुम्हारा नाम रत्नसिंह है; पर तुम मेरे रत्नसिंह नहीं हो।
तुम मेरी तरफ देखो तो, मैं ही तुम्हारा दास, तुम्हारा उपासक, तुम्हारा पति हूं।
'मेरे पति ने वीर गति पायी'।
'हाय! कैसे समझाऊं ! अरे लोगो, किसी भांति अग्नि शांत करो। मैं रत्नसिंह ही हूं, प्रिये ? क्या तुम मुझे पहचानती नहीं हो ?'
अग्निशिखा चिंता के मुख तक पहुंच गयी। अग्नि में कमल खिल गया। चिंता स्पष्ट स्वर में बोली- खूब पहचानती हूं। तुम मेरे रत्नसिंह नहीं। मेरा रत्नसिंह सच्चा शूर था। वह आत्मरक्षा के लिए, इस तुच्छ देह को बचाने के लिए अपने क्षत्रिय धर्म का परित्याग न कर सकता था। मैं जिस पुरुष के चरणों की दासी बनी थी, वह देवलोक में विराजमान है । रत्नसिंह को बदनाम मत करो। वह वीर राजपूत था, वह वीर राजपूत था, रणक्षेत्र से भागने वाला कायर नहीं !
अंतिम शब्द निकले ही थे कि अग्नि की ज्वाला चिंता के सिर के ऊपर जा पहुंची। फिर एक क्षण में वह अनुपम रूप-राशि, वह आदर्श वीरता की उपासिका, वह सच्ची सती अग्नि - राशि में विलीन हो गयी।
रत्नसिंह चुपचाप, हत्बुद्धि-सा खड़ा यह शोकमय दृश्य देखता रहा। फिर अचानक एक ठंडी सांस खींच कर उसी चिता में कूद पड़ा।
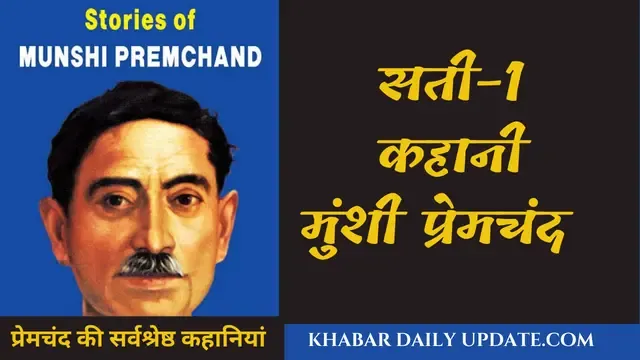
एक टिप्पणी भेजें