भाषाओं का पारस्परिक प्रभाव,भाषा शास्त्र का समीक्षण और परीक्षण
भाषाओं का पारस्परिक प्रभाव- भाषा -शास्त्र का समीक्षण और परीक्षण: परदेशी भाषाएँ न पढ़ने का उपदेश पहले दिया गया था। उसका भी वही परिणाम हुआ, जो अँगरेज़ी शासन काल के प्रारम्भिक काल में अँगरेज़ी भाषा के प्रति अथवा पहले पहल जब जल प्राप्ति के लिए नल लगाये गये थे तब उनके प्रति घृणा की भावना पनपी; अर्थात् सर्वसाधारण ने विरोधियों की बात न मानी और निषेधों का विचार न करके लोग अन्य देशों की भाषाएँ पढ़ते रहे।
यदि ऐसा न किया जाता तो राजधर्म और व्यापार कैसे चलता? 'महाभारत' में हम पढ़ते हैं कि लाक्षागृह के विषय में सचेत करते समय महात्मा विदुर ने युधिष्ठिर से म्लेक्ष-भाषा में सम्भाषण किया है। तात्पर्य यह कि हज़ार रोकथाम करने पर भी भाषाओं का प्रभाव एक-दूसरे पर पड़ ही जाता है।
Read More: भाषा किसे कहते है अर्थ परिभाषाएं और प्रकार | What is Language in Hindi
इस भाषा संघर्ष के समय कितने ही शब्द अपना देश छोड़कर दूसरी जगह जा बसते हैं और कुछ दोनों देशों में अड्डा जमाये रहते हैं। लड़ाई में घायल हो जाने के कारण कुछ का रूप बदल जाता है और कुछ बेचारे अपनी जान से ही हाथ धो बैठते हैं। इसी नियम के अनुसार प्राकृत में भी बहुत से शब्द ऐसे पाये जाते हैं, जिनका पता देववाणी में नहीं मिलता। ये दूसरे देशों के रूप बदले हुए शब्द हो सकते हैं अथवा उस भाषा के हो सकते हैं,जो उन लोगों में बोली जाती थी।
जो आर्यों के यहाँ आने के समय बसे हुए थे किन्तु प्राकृत का भी सब जगह एक ही रूप प्रचलित न था। जिन कारणों से बंगाल के निवासी आज सौम्य को शौम्य और पंजाब के निवासी स्कूल को सकूल तथा आत्म को आतम कहते हैं,उन्हीं अथवा उनसे मिलते-जुलते भाषा-शास्त्र का समीक्षण और परीक्षण किन्हीं दूसरे कारणो से प्राकृत के भी कई रूप दिखायी देने लगे थे यद्यपि उनमें समानता अधिक थी। जब प्राकृत में साहित्य रचना होने लगी तब बोल चाल की भाषा और उसमें भेद हो गया।
इसी प्रकार प्राकृत ने कई रूप बदले। उसका दूसरा व्यापक रूप पालि है,जो गौतम बुद्ध के सम्बन्ध के कारण सबसे महत्त्व का माना जाता है। पालि में भी बहुत कुछ साहित्य रचना हुई। उस समय के जो शिलालेख ताम्र पत्र आदि मिलते हैं,उनसे पालि के भिन्न-भिन्न रूपों का कुछ हाल ज्ञात हो सकता है। यहाँ हम पहली प्राकृत से दूसरी प्राकृत यानी पालि का सम्बन्ध दिखाकर व्यर्थ आपका समय लेना नहीं चाहते।
Read More: आर्य भाषा प्रकार,वर्गीकरण और विश्व - भाषा का विभाजन एक विश्लेषणात्मक अध्ययन
हाँ,इतना अवश्य बता देना चाहते है कि बोल-चाल की भाषा होने और साहित्य रचना के लिए बहुत पुरानी न होने पर भी प्राकृत किसी समय अगणित अलंकारों से सजी हुई संस्कृत से अधिक मधुर और चमत्कृत समझी जाती थी और वह भी मूों में नहीं बल्कि उद्भट विद्वानों में। राजशेखर ने कर्पूरमञ्जरी में लिखा है ,
"परुसा सक्क अबन्धा पाउ अबन्धो विहोई सुउमारो
पुरुस महिलाणं जेन्ति अमिह अन्तरं तेतिय मिमाणं।"
इसका अर्थ यह है कि संस्कृत की रचना 'कठोर' और प्राकृत की 'सुकुमार' होती है। इन दोनों भाषाओं में पुरुष और स्त्री में बराबर अन्तर है।
कालान्तर में , विद्वानों ने देश-भेद से प्राकृत के शौरसेनी,मागधी और महाराष्ट्री- ये तीन अपभ्रंश माने थे । उस समय दक्षिण-पश्चिम में प्रचलित नागर नाम का भी एक अपभ्रंश माना जाता था,जिससे कुछ लोगों की राय में महाराष्ट्री और शौरसेनी की उत्पत्ति हुई। कुछ विद्वान् 'मागधी को शौरसेनी' का अपभ्रंश बताते हैं तो कुछ मागधी ' को मूल प्राकृत जबकि कुछ 'महाराष्ट्री' को मूल प्राकृत। 'शौरसेनी' और 'मागधी' के मेल से उत्पन्न 'अर्द्धमागधी' नाम की एक अपभ्रंश भाषा थी,जिससे पूर्वी हिन्दी का विकास हुआ।
Read More: व्याकरण अर्थ परिभाषा और हिन्दी भाषा से अन्तर्सम्बन्ध
हमारे विचार में तो यह भी एक क्रान्ति का युग था और इन अपभ्रंशों में पारस्परिक समानता और असमानता देखकर ही विद्वानों ने “अपनी-अपनी डफली अपना-अपना राग” वाली कहावत चरितार्थ की है। यदि ‘मागधी' (जिससे बिहारी की सृष्टि हुई है) के पूर्व-रूप को बौद्ध-धर्म के कारण विशेष महत्त्व मिला तो अर्द्धमागधी को महावीर स्वामी और दूसरे जैन तीर्थंकरों के कारण उतना ही महत्त्व प्राप्त हुआ था।
हिन्दी-संसार में मैथिली का भी स्थान है यद्यपि प्राच्य प्राकृत से उत्पन्न होने के कारण यह बॉग्ला भाषा की सगी बहन है। प्रख्यात भाषाविद् डॉ० ग्रियर्सन की अवधारणा है- शौरसेनी तथा अर्द्धमागधी के मेल से ही वर्तमान हिन्दी की सृष्टि हुई है।
डॉ० ग्रियर्सन यह सम्मति और भी कितने ही विद्वान् लेखकों ने मान ली है परन्तु हमारा विश्वास है कि वर्तमान हिन्दी पर पंजाबी का पूरा प्रभाव पड़ा है। इस विश्वास की पुष्टि में कितने ही उदाहरण दिये जा सकते हैं। संस्कृत की यास्यति क्रिया का प्राकृत रूप जाएज्जा है।
Read More: वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत भाषा व् भाषा का जीवन्त रूप
पंजाबी में इसका अपभ्रंश जाएगा अथवा जावेगा है,जो कि आजकल बोल-चाल की हिन्दी में आता है। शौरसेनी से विकसित ब्रजभाषा में जाएगौ कहेंगे और अर्द्धमागधी के विकसित रूप में जैहै अथवा जइहै। ब्रज भाषा में जहाँ घोडौ कहा जाता है,वहाँ पंजाबी में घोड़ा और इसी रूप में आधुनिक हिन्दी में भी बोला जाता है।पंजाबी का प्रभाव हिन्दी पर बांगड़ बोली की कृपा से पड़ा,जो दिल्ली और पंजाब तथा दिल्ली और राजस्थान के बीच की भाषा है। जिस राज्य में यह बोली जाती है, उसे 'हरियाणा' कहते हैं। इस पर राजस्थानी का भी प्रभाव पड़ा है।
नीचे डॉ ० ग्रियर्सन के ' LLinguistic Survey of India ' नामक ग्रन्थ में से इसका एक उदाहरण दिया गया है, "एक माणस कै दो छोरे थे। उनमैं तै छोट्टे ने बाप्पू तै कह्या अक बाप्पू हो धन का जौणसा हिस्सा मेरे बाँडे आवे सै मन्नै दे दे।"
इसी से मिलती-जुलती भाषा दिल्ली के आसपास तथा और भी कई जगह बोली जाती है । इधर, आगरा की बोलचाल की भाषा पर ध्यान देने से भी खड़ी बोली की उत्पत्ति शौरसेनी + अर्द्धमागधी तथा पंजाबी + पैशाची के अपभ्रंश से सिद्ध हो जाती है। पंजाबी के सम्बन्ध में यह आत ध्यान में रखने योग्य है कि इसकी उत्पत्ति पंजाबी-प्राकृत तथा पैशाची के मेल से हुई है। पैशाची, जिसे 'भूत-भाषा' भी कहते थे, उत्तर-पंजाब में,कश्मीर की ओर बोली जाती थी। कुछ विद्वानों की राय में वह मध्यप्रदेश और राजपूताने के आसपास बोली जाती थी परन्तु प्रमाणों से यह बात सिद्ध नहीं होती। संस्कृत और प्राकृत से उसका क्या सम्बन्ध था, यह दिखाने के लिए कुछ उदाहरण देने अनुचित न होगे।
Read More: भाषा शब्द - शास्त्र का तुलनात्मक अध्ययन
संस्कृत | प्राकृत | पैशाची |
दुष्ट: | दुट्ठ | दुसट |
कष्ट: | कट्ठ | कसट |
सहते | सहड़ | सहदे |
इन उदाहरणो से सूचित होता है कि पैशाची का लगाव संस्कृत से अधिक है, प्राकृत से कम। ऊपर के उदाहरण में सहदे दिया हुआ है; इसी अर्थ में आधुनिक हिन्दी में सहते ( हैं ) कहेंगे। 'सहइ' तो प्राकृत का रूप है, जो ब्रज-भाषा में 'सहहि' का रूप धारण कर लेगा। हाँ,आगरा की बोली के प्रभाव के कारण सहै है- सरीखे रूप में भी उसमें आते रहे हैं। इस उदाहरण यह प्रमाणित हो जाता है कि खड़ी बोली की क्रियाएँ किधर से आयी हैं। इनमें से एक रूप ( सहता,करता आदि ) का वंश-वृक्ष देखने से अर्द्धमागधी और शौरसेनी का कहीं पता भी नहीं मिलता। ऐसे और भी उदाहरण दिये जा सकते हैं।
अवन्ती में प्राकृत का जो रूप प्रचलित था,उसी से कुछ सज्जन राजस्थानी की और उसी से मिलते-जुलते एक और रूप गोर्जरी से गुजराती की उत्पत्ति मानते हैं। इसमें सन्देह नहीं कि राजस्थानी और गुजराती का तुलनात्मक अध्ययन करने से दोनों का विकास एक ही स्थान से हुआ दिखता है। राजपूताने के कुछ भागों की बोली और इधर मालवा की बोली से गुजराती की बहुत अधिक समता है। इससे उल्लिखित सिद्धान्त की और भी पुष्टि हो जाती है । ब्रज-भाषा और राजस्थानी में जो समता दिखती है,उसका कारण इन दोनों ही का नागर अपभ्रंश से उत्पन्न होना हो सकता है क्योंकि शौरसेनी को भी कुछ विद्वानों ने नागर अपभ्रंश का ही एक भेद माना है।इसी तरह प्राकृत के अवन्तीबाला रूप भी,जिससे राजस्थानी की उत्पत्ति हुई बतायी जाती है,नागर अपभ्रंश का ही एक भेद कहा जाता है।
पूर्वी हिन्दी- बैसवाड़ी ( जिसको अवधी भी कहते हैं ) और बघेलखण्ड तथा छत्तीसगढ़ में बोली जानेवाली भाषाओं की उत्पत्ति ‘अर्द्ध-मागधी' से है, जो कि 'मागधी' और 'शौरसेनी' का घोटाला है।
भाषाओं के इस प्रकरण पर विचार करते समय यह बात न भूलनी चाहिए कि इन सबकी मूल भाषा एक ही थी और इसी कारण अनेक अपभ्रंश हो जाने पर भी सबमें समानता की एक लहर प्रवाहित हुई,जो कि अब भी देखी जा सकती है। उदाहरणार्थ, करता हूँ के अर्थ में करदा भाषा-शास्त्र का समीक्षण और परीक्षण हाँ, करत हौ, करू लूं, करि आदि एक ही से अथवा एक दूसरे से बहुत कुछ मिलते-जुलते सब राज्यीय बोलियो में मिलेगे। इसी प्रकार और भी कितनी ही सज्ञाओ, सर्वनामो तथा क्रियाओं के उदाहरण दिये जा सकते हैं। अब अपभ्रंश से हिन्दी का सम्बन्ध दिखाने के लिए नीचे कुछ उदाहरण दिये गये है:-
|
प्राकृत |
अपभ्रंश |
हिन्दी |
|
सामलो |
सामलो |
सामलो , साँवरो.साँवला |
|
घोड़ो |
घोडो |
घोडौ घोड़ा |
|
सहते |
सहड़ |
सहदे |
|
एसो |
एहो |
एह इह, यह |
|
ह |
हउँ |
हूँ.हाँ |
|
को |
कवण |
कवन, कौन |
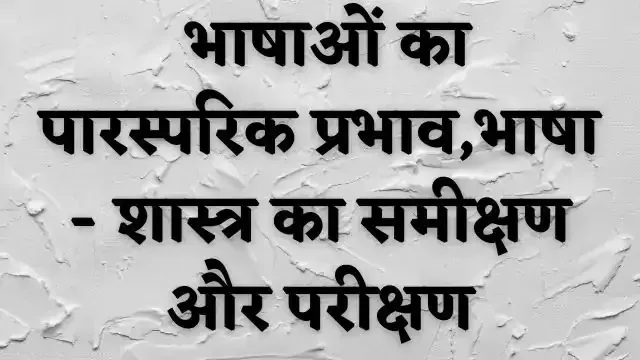
एक टिप्पणी भेजें